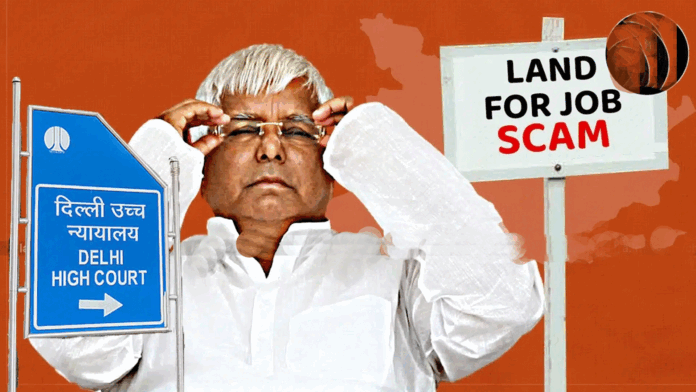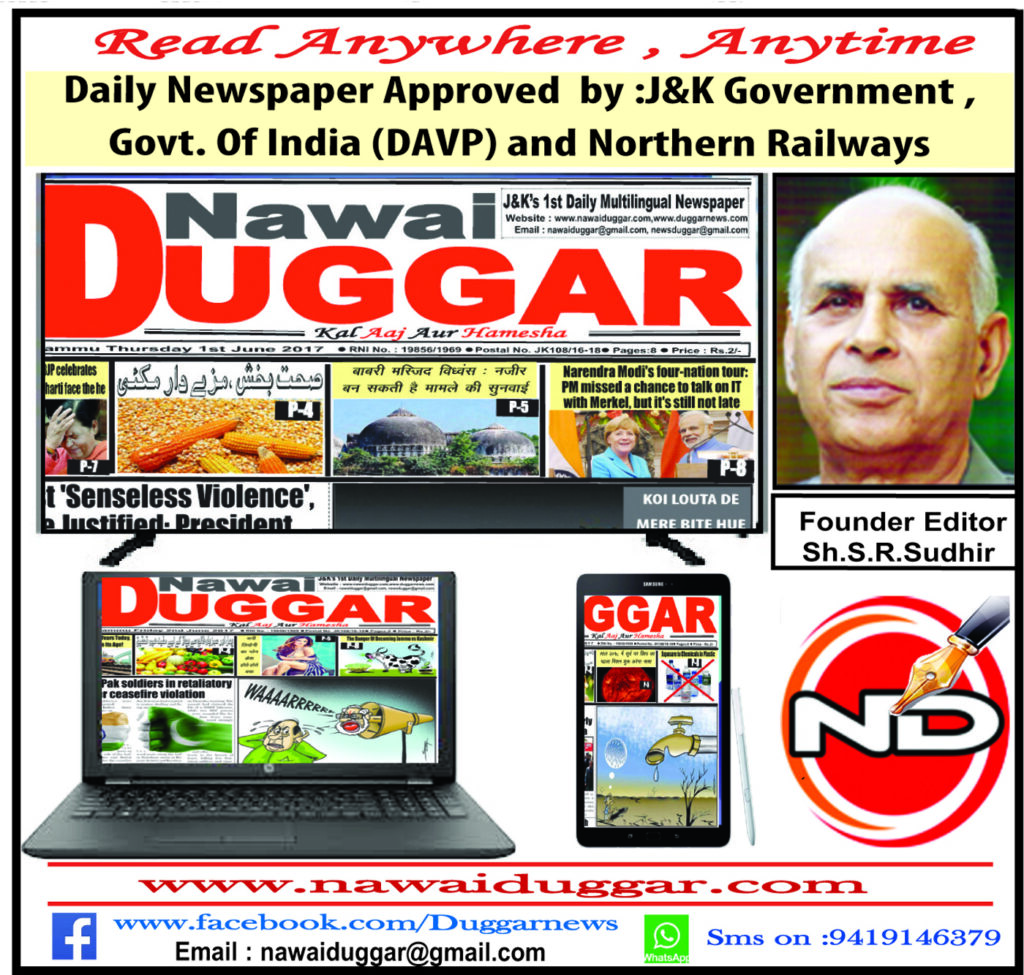नई दिल्ली, 11 सितंबर: खुद को “संविधान का संरक्षक” बताते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पूछा कि अगर राज्यपाल जैसा संवैधानिक पदाधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहता है, तो क्या वह “हाथ पर हाथ धरे बैठे” रह सकता है। साथ ही, उसने विधेयकों को मंज़ूरी देने के राष्ट्रपति के संदर्भ पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
10 दिनों तक चली मैराथन सुनवाई में, मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, अभिषेक सिंघवी, गोपाल सुब्रमण्यम, अरविंद दातार सहित कई कानूनी दिग्गजों को राष्ट्रपति के संदर्भ पर सुना। यह संदर्भ अनुच्छेद 200 और 201 पर केंद्रित था और इस प्रमुख मुद्दे पर भी कि क्या संवैधानिक न्यायालय राज्यपालों और राष्ट्रपति के लिए विधेयकों को मंज़ूरी देने के लिए समयसीमा निर्धारित कर सकता है।
आखिरी दिन, जब मेहता ने शक्तियों के पृथक्करण को संविधान के मूल ढाँचे में से एक बताया, तो पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति एएस चंदुरकर भी शामिल थे, ने उन्हें टोक दिया। मेहता ने कहा कि न्यायालय को समय-सीमा तय नहीं करनी चाहिए और राज्यपालों की विवेकाधीन शक्तियों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। मुख्य
न्यायाधीश ने पूछा, “कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी ऊँचा पद क्यों न रखता हो, संविधान के संरक्षक के रूप में (सुप्रीम कोर्ट का संदर्भ देते हुए)… मैं सार्वजनिक रूप से कहता हूँ कि मैं शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखता हूँ और हालाँकि न्यायिक सक्रियता होनी चाहिए, लेकिन न्यायिक आतंकवाद या दुस्साहस नहीं होना चाहिए। लेकिन साथ ही, अगर लोकतंत्र का एक अंग अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में विफल रहता है, तो क्या संविधान का संरक्षक शक्तिहीन होकर निष्क्रिय बैठा रहेगा?”
मेहता ने कहा, “केवल न्यायालय ही नहीं, कार्यपालिका भी नागरिकों के मौलिक अधिकारों की संरक्षक है… विधायिका भी एक संरक्षक है, तीनों अंग।” विधि अधिकारी ने आगे कहा, “लेकिन, किसी समन्वित संवैधानिक पदाधिकारी के विधायी विवेकाधीन कार्यों के संबंध में राज्यपालों को परमादेश (किसी व्यक्ति को सार्वजनिक कर्तव्य निभाने के लिए कहने वाला आदेश) जारी करना शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन होगा और शक्तियों का यह पृथक्करण मूल संरचना का एक हिस्सा है।” मेहता ने कहा कि राज्यपाल किसी विधेयक पर हमेशा के लिए नहीं बैठ सकते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अनुच्छेद 200 के तहत उनके पास विवेकाधीन शक्तियाँ नहीं हैं और “स्ट्रेटजैकेट फ़ॉर्मूले” के तहत स्वीकृति देने के लिए समय-सीमा तय की जा सकती है।
उन्होंने राज्य सरकार द्वारा अध्यादेश जारी करने के मामले में भी राज्यपालों की विवेकाधीन शक्तियों को रेखांकित किया।
विपक्ष शासित राज्यों की इस दलील पर तीखा हमला करते हुए कि राज्यपाल को केवल मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर ही कार्य करना चाहिए, मेहता ने पूछा, “मान लीजिए कि कोई राज्य विधानमंडल एक विधेयक पारित करता है जिसमें घोषणा की जाती है कि वह अब भारत संघ का हिस्सा नहीं रहेगा, तो राज्यपाल के पास स्वीकृति रोकने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।” उन्होंने कुछ संदर्भों में राज्यपालों और राष्ट्रपति को संवैधानिक विवेकाधिकार दिए जाने की बात पर जोर दिया, हालांकि उन्होंने कहा कि उनके कार्य सामान्यतः मंत्रिस्तरीय सहायता और सलाह से निर्देशित होते हैं।
उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 200 राज्यपाल को विधेयकों पर चार विकल्प प्रदान करता है और इसमें निहित विवेकाधिकार निहित है, खासकर उन स्थितियों में जहाँ कोई विधेयक संवैधानिक मूल्यों को कमज़ोर करता है या राष्ट्रीय निहितार्थ रखता है।
विधि अधिकारी ने कहा कि अनुच्छेद 200 में प्रयुक्त “यथाशीघ्र” शब्द का अर्थ अनिश्चित काल तक नहीं हो सकता।
उन्होंने दोहराया कि 1970 से राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित 90 प्रतिशत विधेयकों को एक महीने के भीतर राज्यपाल की स्वीकृति मिल गई है, जबकि कुल 17,150 विधेयकों में से केवल 20 मामलों में ही राज्यपालों ने अपनी स्वीकृति रोकी है।
संवैधानिक पाठ में स्पष्ट समय-सीमा के अभाव पर बात करते हुए, मेहता ने कहा कि यह शून्यता के बजाय “शब्दों के सतर्क चयन” को दर्शाता है। उन्होंने कहा
, “यह व्यवस्था दशकों से सामंजस्य के साथ काम करती रही है। हाल ही में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली प्रकरण के साथ, इस मुद्दे पर मुकदमेबाजी में तेज़ी आई है।” उन्होंने
कहा कि संवैधानिक व्यवस्था में कोई शून्यता नहीं है जहाँ न्यायालय को हस्तक्षेप करना चाहिए और राज्यपालों के लिए समय-सीमा तय करनी चाहिए।
न्यायालय संभवतः राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा संदर्भित 14 प्रश्नों पर अपनी राय देगा, जिनमें यह भी शामिल है कि क्या संवैधानिक प्राधिकारी विधेयकों पर अनिश्चित काल तक स्वीकृति रोक सकते हैं और क्या न्यायालय अनिवार्य समय-सीमाएँ निर्धारित कर सकते हैं।
ये मुद्दे मूलतः अनुच्छेद 200 से संबंधित हैं, जो राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों के संबंध में राज्यपाल की शक्तियों को नियंत्रित करता है, जिससे उन्हें विधेयक पर स्वीकृति देने, स्वीकृति रोकने, विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस करने या राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को आरक्षित करने का अधिकार प्राप्त होता है।
मई में, राष्ट्रपति मुर्मू ने अनुच्छेद 143(1) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए शीर्ष न्यायालय से यह जानने का प्रयास किया था कि क्या न्यायिक आदेश राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों पर विचार करते समय राष्ट्रपति द्वारा विवेकाधिकार के प्रयोग के लिए समय-सीमाएँ निर्धारित कर सकते हैं।